नई दिल्ली। भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए, नो-डिटेंशन पॉलिसी के तहत कक्षा 5 और 8 में छात्रों को फेल करने का प्रावधान फिर से लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पहले यह नीति लागू थी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था, चाहे वे परीक्षा में पास हों या नहीं। अब, नए संशोधन के अनुसार, छात्र अगर फेल होते हैं, तो उन्हें सुधारात्मक परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। असफल होने पर, उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
सरकार का तर्क है कि यह कदम छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पास-फेल प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, शिक्षा में जीवन कौशल और समग्र विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
शिक्षा प्रणाली में बदलाव क्यों :-
नो-डिटेंशन पॉलिसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शिक्षा सभी तक पहुँचे और छात्रों को विफलता के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता बढ़ी कि इस नीति से सीखने के परिणामों में गिरावट आ रही है। नए प्रावधानों के तहत:
- फेल होने के बाद दोबारा परीक्षा का मौका : कक्षा 5 और 8 के छात्रों को, असफल होने पर, 2 महीने के भीतर सुधारात्मक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।
- सुधारात्मक सहायता : छात्रों को अकादमिक सहायता और काउंसलिंग दी जाएगी ताकि वे सीखने के अंतर को पाट सकें।
- उत्तरदायित्व : स्कूल और शिक्षक, छात्रों की प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।
जीवन कौशल की आवश्यकता
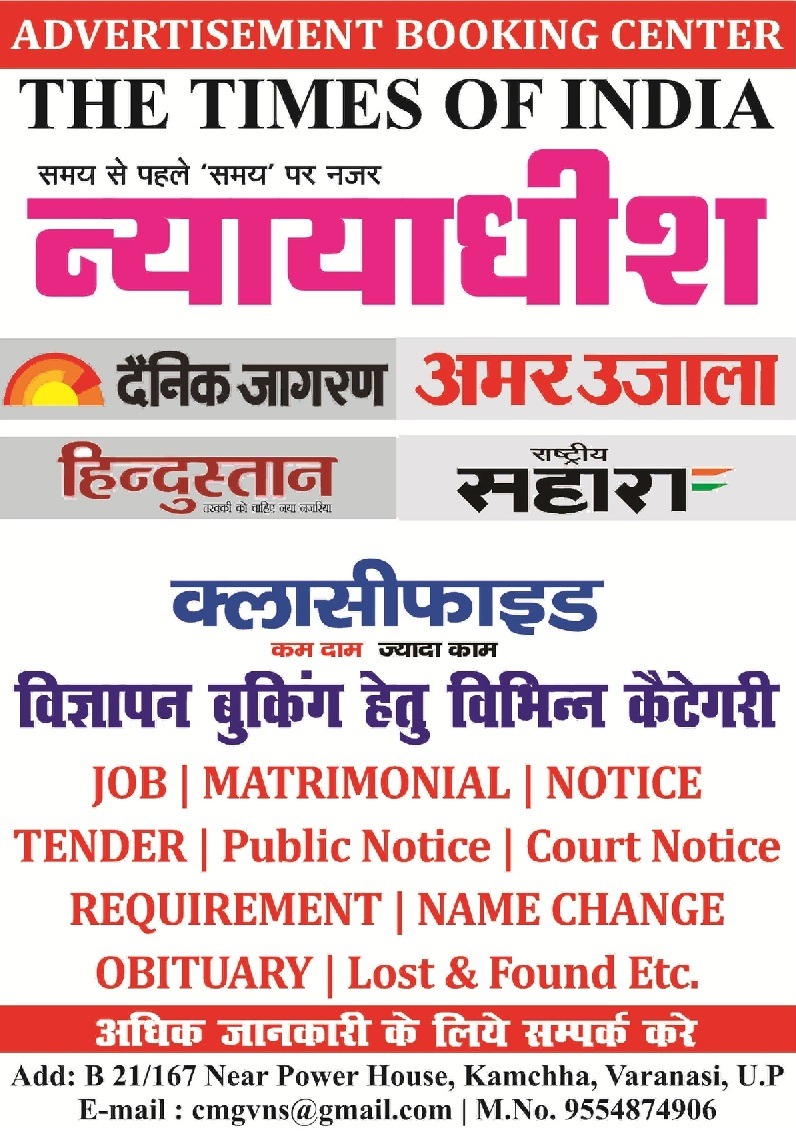
विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा नीति केवल परीक्षा के परिणामों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जीवन के व्यावहारिक और सामाजिक कौशल प्रदान करना होना चाहिए।
- मनोवैज्ञानिक समर्थन : दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों में स्कूल अब संघर्षरत छात्रों को शैक्षणिक सुधार के साथ-साथ भावनात्मक समर्थन भी प्रदान कर रहे हैं।
- योग्यता-आधारित मूल्यांकन : केंद्रीय और सैनिक स्कूलों में रटने की बजाय छात्रों की व्यावहारिक ज्ञान और समझ को प्राथमिकता दी जा रही है।
- माता-पिता की भागीदारी : अभिभावकों को भी बच्चों की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है :-
- शिक्षकों का प्रशिक्षण : शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और सुधारात्मक उपायों में प्रशिक्षित किया जाए।
- मूलभूत कौशल पर ज़ोर : छात्रों को केवल परीक्षा में पास करने के लिए तैयार करने के बजाय, उन्हें संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और टीमवर्क सिखाया जाए।
- सुधारात्मक संरचनाएँ : स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ और कोचिंग प्रदान की जाए।
सरकार के प्रयास सीखने के स्तर को सुधारने के लिए हैं, लेकिन शिक्षा को केवल पास-फेल प्रणाली तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है। समय की माँग है कि छात्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाए और जीवन कौशल सिखाने की नीति बनाई जाए। यदि इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह न केवल शिक्षण प्रणाली को सुधार सकता है, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी उज्जवल बना सकता है।
